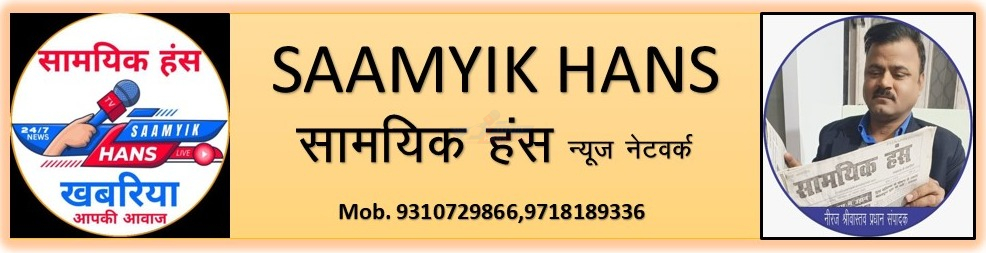एक मां जो पहली बार डेथ कैफे में रोई, क्या होते हैं ये जो लोगों की जिंदगी संवार देते हैं, भारत में ये कहां, इनके किस्से

आपने कई तरह के कैफे के बारे में सुना होगा लेकिन शायद डेथ कैफे के बारे में नहीं. चौंकिए मत. ये भी एक अलग तरह का कैफे है. यहां भी लोग आते हैं. कॉफी की चुस्कियां लगाते हैं लेकिन साथ में करते क्या हैं. ये जानना जरूर दिलचस्प हो सकता है क्योंकि इस कैफे का नाम ही डेथ कैफे है. ये क्या है. कैसे इसे ये नाम मिला. किसने इसे शुरू किया. भारत में भी क्या ऐसे कैफे हैं.
दुनिया में पारंपरिक कैफों की संख्या तो लाखों में हो सकती है. यहां लोग आते हैं कॉफी, स्नैक्स और अखबार के साथ समय बिताते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं.ये कैफे सामाजिक संवाद और आराम के लिए होते हैं. इसके अलावा साइबर कैफे, कैट कैफे, डॉग कैफे, मर्डर मिस्ट्री कैफे, साइलेंट कैफे, नैप कैफे होते हैं. कई जगह बुक कैफे मिल जाएंगे लेकिन अब डेथ कैफे भी होते हैं. बेशक इनकी संख्या कम हो लेकिन ये पूरी दुनिया में मिल जाएंगे.
दरअसल डेथ कैफे इसी जगह है जहां लोग एक अनौपचारिक माहौल में बैठकर मृत्यु, जीवन और मृत्यु से जुड़ी भावनाओं पर खुलकर बात करते हैं. इसका उद्देश्य लोगों को मृत्यु के बारे में सोचने, उसे स्वीकारने और जीवन को और गहराई से समझने में मदद करना है.
डेथ कैफे क्या होता है?
यह कोई धार्मिक अनुष्ठान या थेरेपी सेशन नहीं होता ना ही यहां किसी को मौत के बारे में डराया जाता है. इसमें लोग आमतौर पर चाय-कॉफी और केक के साथ बैठते हैं. मृत्यु से जुड़े अनुभव, भय, सवाल, दर्शन या व्यक्तिगत किस्से साझा करते हैं. बातचीत सहज, खुले, बिना जजमेंट के माहौल में होती है. इसका कोई तय एजेंडा, थीम या प्रचार नहीं होता – बस एक मुक्त और संवेदनशील चर्चा.
– कोई तय एजेंडा नहीं होता
– कोई प्रचार या व्याख्यान नहीं दिया जाता
– कोई विशेषज्ञ या गुरु मौजूद नहीं होता
– हर व्यक्ति को बोलने और सुनने की बराबर आज़ादी होती
सत्र आमतौर पर एक सामान्य कैफे या पुस्तकालय जैसी जगह पर, चाय, कॉफी और मिठाई के साथ आयोजित किया जाता है, जिससे वातावरण सहज और मैत्रीपूर्ण बना रहे
आइए डेथ कैफे को पूरी तरह जानने से पहले इनके कुछ किस्सों को भी जान लेते हैं, जो सच हैं और जिनसे लोगों की जिंदगियां बदल गईं.
लंदन की मां की कहानी, जो पहली बार रोई
एक लंदन निवासी महिला, जिनका 19 वर्षीय बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया, वर्षों तक गहरे शोक में थीं. कभी किसी से बात नहीं की. जब वो पहली बार डेथ कैफे में गईं तो शुरू में चुप रहीं. लेकिन जैसे-जैसे और लोग अपने अनुभव साझा करने लगे, उन्होंने भी बेटे की कहानी साझा की. बात खत्म होते ही वे ज़ोर से रोने लगीं.
उन्होंने कहा, “यह पहली जगह थी जहां मुझे लगा कि मैं एक मां हूं, सिर्फ दुख की मूरत नहीं. मैं रोयी, लेकिन डर के बिना.” बाद में वे डेथ कैफे में रेगुलर आने लगीं. दूसरों को सांत्वना देना उनका मक़सद बन गया.
मैं मरने से नहीं, अधूरे जीवन से डरता हूं”
2019 में दिल्ली में आयोजित एक डेथ कैफे में एक 29 वर्षीय युवक ने कहा, “मैं जीवन को लेकर इतना उलझा हूं कि कभी मृत्यु के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला. लेकिन यहां आने के बाद मुझे लगा कि असल डर मौत का नहीं, एक अधूरे, व्यर्थ जीवन का है.”
उस बातचीत ने उसे प्रेरित किया कि वह अपने अधूरे उपन्यास को पूरा करे. 6 महीने बाद उसने वही उपन्यास एक छोटे पब्लिशर से छपवाया.
“हमने दादी की इच्छाओं को गंभीरता से लेना सीखा”
बेंगलुरु के एक डेथ कैफे में एक परिवार की तीन पीढ़ियां शामिल हुईं – दादी, उनकी बेटी और पोती. दादी ने साफ शब्दों में कहा कि वो ICU में मरना नहीं चाहतीं, न ही लंबी मशीनों से बंधकर.
उन्होंने कहा, “मुझे मेरी तुलसी के नीचे बैठने दो आखिरी दिन, ना कि हॉस्पिटल के उजले मगर अकेले बिस्तर पर.” उनकी बेटी जो डॉक्टर थीं, हैरान रह गईं. उन्हें कभी लगा ही नहीं कि मां की मौत को लेकर स्पष्ट राय हो सकती है. उस दिन के बाद उन्होंने मृत्यु से पहले की इच्छाओं का लिखित दस्तावेज बनवाया.
“मैं आत्महत्या नहीं चाहता, बस कोई सुनने वाला चाहिए”
जापान में एक युवक, जो आत्महत्या के विचार से जूझ रहा था, डेथ कैफे में पहुंचा. वहां उसने कहा, “मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन जीने का कारण भी नहीं मिल रहा था. यहां पहली बार किसी ने मुझे टोका नहीं, जज नहीं किया, बस सुना.” उसने 3 महीने बाद एक मेल भेजा कि वो अब थेरेपी ले रहा है. उसके शब्द थे, “मुझे लगा मेरी मृत्यु से पहले मेरी कहानी कोई सुने – बस वही राहत थी.”
“डेथ कैफे ने मेरी किताब को जन्म दिया”- कोलकाता लेखिका
कोलकाता में एक लेखिका अपने पिता की मृत्यु के बाद गहरे अवसाद में थीं, वह एक डेथ कैफे में गईं. वहां उन्होंने अपने अनुभव को शब्दों में ढालना शुरू किया – एक कागज़ पर कविता, फिर संस्मरण.
उन्होंने कहा, “मृत्यु के बारे में लिखने की शक्ति मुझे मृत्यु की गोद से ही मिली. और डेथ कैफे वह पालना था.” बाद में उनकी किताब “शव, शब्द और शांति” एक स्वतंत्र पब्लिशर से प्रकाशित हुई. बहुत सराही गई.
डेथ कैफे की शुरुआत कैसे हुई?
2011 में ब्रिटेन के जॉन अंडरवुड और उनकी मां सुज़ी विल्मेंट ने यह कॉन्सेप्ट शुरू किया. वे बौद्ध दर्शन और स्विस समाजशास्त्री बर्नार्ड क्रेत्ताज़ से प्रभावित थे, जिन्होंने मृत्यु पर सार्वजनिक चर्चा की वकालत की थी. उन्होंने मृत्यु पर सार्वजनिक चर्चा को समाज के लिए जरूरी बताया था. जॉन ने अपने घर के तहखाने में पहला डेथ कैफे आयोजित किया, जहां कुछ लोगों ने चाय और केक के साथ बैठकर मृत्यु पर चर्चा की. इस पहल को ऑनलाइन साझा करने के बाद यह विचार दुनियाभर में फैलने लगा. अब तक दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में 15,000 से ज्यादा डेथ कैफे हो चुके हैं.
क्या भारत में डेथ कैफे का चलन है
हां, भारत में भी डेथ कैफे धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं, खासकर बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई जैसे शहरों में. बेंगलुरु में कुछ मानसिक स्वास्थ्य संगठनों और व्यक्तिगत पहल से डेथ कैफे हुए हैं. दिल्ली में 2019 में पहला औपचारिक डेथ कैफे आयोजित किया गया था जिसमें लेखकों, मनोचिकित्सकों और आम लोगों ने हिस्सा लिया.
हालांकि भारत में मृत्यु को लेकर बात करना अभी भी वर्जित और असहज विषय माना जाता है, लेकिन शहरी, शिक्षित वर्ग में इसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है.
इनमें क्या बातें होती हैं?
लोग अपने परिजनों की मृत्यु के अनुभव साझा करते हैं. कोई मरने के डर, आत्महत्या के विचार या जीवन की अस्थिरता पर बात करता है. हिंदू, बौद्ध, इस्लामिक या अन्य धार्मिक मृत्यु पर सोचने विचारने और उनकी परंपराओं की तुलना की जाती है. इसमें अंत समय में केयर, मृत्यु की तैयारी, वसीयत, इच्छा मृत्यु जैसे विषय आते हैं. कई बार कलाकार, कवि या लेखक मृत्यु विषय से जुड़ी रचनाएं पढ़ते या सुनाते हैं.
क्यों ज़रूरी हैं डेथ कैफे?
मृत्यु के डर को सामान्य करना. हम मृत्यु को जितना टालते हैं, वह उतनी ही डरावनी लगती है. डेथ कैफे उसे सामान्य विषय बनाकर भय को कम करता है.
मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है. दुःख, अकेलापन और अवसाद जैसे अनुभवों को साझा करने से राहत मिलती है. जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है. सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है. अनजान लोग भी ऐसी बातचीत के दौरान गहराई से एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं.
डेथ कैफे को लेकर गलतफहमियां हैं?
कुछ लोग इसे अंधविश्वास या आत्महत्या को बढ़ावा देने वाला मानते हैं, जबकि यह पूरी तरह स्वेच्छा और समर्थन आधारित होता है. यह थेरेपी या इलाज नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और दार्शनिक संवाद का मंच है